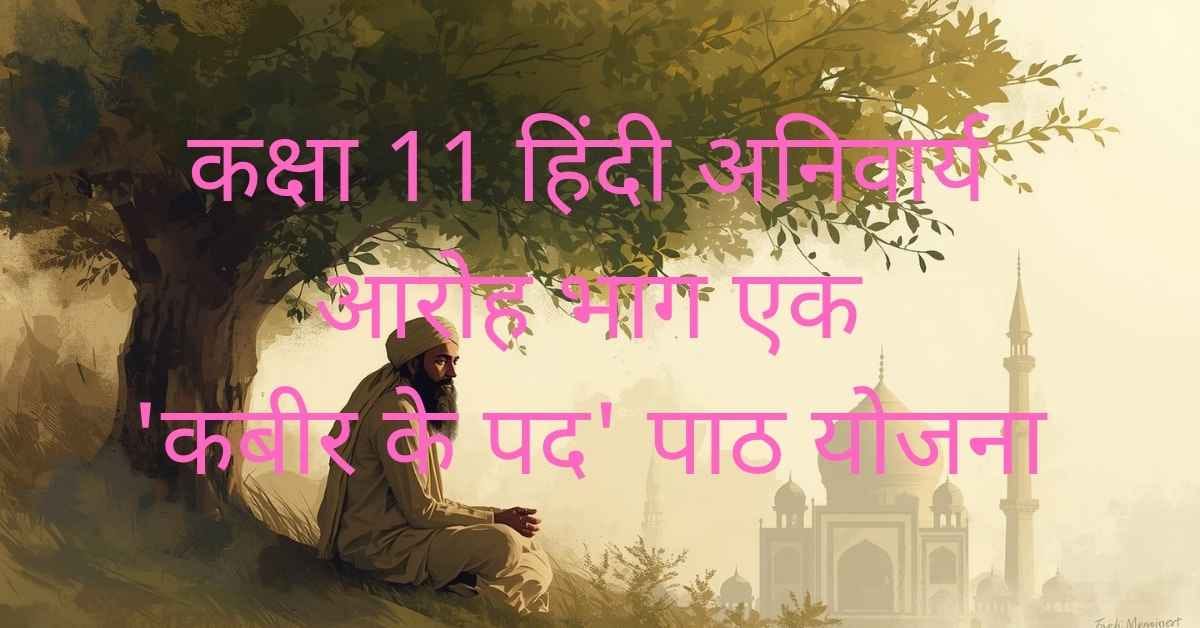कबीर पाठ योजना | Kabir Path Yojana | आरोह भाग-1 | कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य
नमस्कार शिक्षक साथियों! ‘हिंदी की पाठशाला’ के ‘शिक्षक कॉर्नर’ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए RBSE कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की NCERT पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग-1’ के काव्य खंड से भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि ‘कबीर’ के पद “हम तौ एक एक करि जांनां” पर आधारित एक विस्तृत और गहन पाठ योजना लेकर आए हैं। यह Kabir Path Yojana आपके कक्षा शिक्षण को प्रभावी और सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि आपको विस्तृत व्याख्या, दार्शनिक विश्लेषण, NCERT समाधान और परीक्षा-केंद्रित अभ्यास जैसी सभी आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर मिल सके।
इस लेख में आप क्या पढ़ेंगे
पाठ अवलोकन
| विवरण | जानकारी |
| कक्षा | 11 |
| विषय | हिंदी (अनिवार्य) |
| पुस्तक | आरोह भाग-1 (काव्य खंड) |
| पाठ | 1. कबीर (पद: हम तौ एक एक करि जांनां) |
| कवि | कबीर |
| अनुमानित समय | 45 मिनट (1 कालांश) |
शैक्षणिक उद्देश्य एवं सामग्री
सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)
- विद्यार्थी कबीर के अद्वैतवादी दर्शन (ईश्वर एक है) को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कबीर के विचारों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- विद्यार्थी पद में प्रयुक्त रूपकों (कुम्हार, बढ़ई) और दृष्टांत अलंकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- विद्यार्थी RBSE परीक्षा पैटर्न के अनुसार सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे।
आवश्यक सामग्री (Required Materials)
- पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग-1’
- श्यामपट्ट/व्हाइटबोर्ड और मार्कर/चॉक
- कबीर के जीवन और दर्शन से संबंधित चार्ट (वैकल्पिक)
कवि परिचय: कबीर
1. जीवन परिचय
कबीर का जन्म सन् 1398 में वाराणसी के पास ‘लहरतारा’ (उत्तर प्रदेश) में हुआ माना जाता है। वे भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, जैसा कि उनकी पंक्ति “मसि कागद छुयो नहिं, कलम गही नहिं हाथ” से स्पष्ट है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ही ज्ञान अर्जित किया और किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनका देहांत सन् 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ।
2. साहित्यिक परिचय
कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त कर्मकांड, बाह्य आडंबर, जाति-भेद और सांप्रदायिक भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। वे प्रेम, सद्भाव और समानता के समर्थक थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में, प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें ‘वाणी का डिक्टेटर’ कहा है।
3. प्रमुख रचनाएँ
कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा ‘बीजक’ नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसके तीन भाग हैं- साखी, सबद और रमैनी। यहाँ प्रस्तुत पद ‘कबीर वाङ्मय – खंड 2 (सबद)’ से लिया गया है।
4. भाषा-शैली
कबीर की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी, जिसमें हिंदी की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। उनकी भाषा को ‘सधुक्कड़ी’ या ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा जाता है। उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए दृष्टांतों और रूपकों का सुंदर प्रयोग किया है, जिससे उनका काव्य अत्यंत प्रभावशाली बन गया है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (कक्षा के लिए विस्तृत गाइड)
1. पूर्व ज्ञान से जोड़ना (Engage – 5 मिनट)
कक्षा की शुरुआत इन दार्शनिक प्रश्नों से करें ताकि विषय के प्रति छात्रों की जिज्ञासा जागृत हो सके:
- ईश्वर के स्वरूप के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ईश्वर एक है या अनेक?
- क्या सभी मनुष्यों में कोई एक समान तत्व है जो उन्हें जोड़ता है?
- समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?
2. पाठ की प्रस्तुति (Explore & Explain – 20 मिनट)
सस्वर वाचन: उचित भाव, लय और आरोह-अवरोह के साथ पद का सस्वर वाचन करें।
पद की विस्तृत व्याख्या:
पंक्तियाँ 1-4: “हम तौ एक एक करि जांनां… एकै कोहरा सांनां॥”
शब्दार्थ: दोइ – दो, तिनहीं – उनको, दोजग – नरक, नाहिंन – नहीं, जोति – प्रकाश, खाक – मिट्टी, भांडै – बर्तन, कोहरा – कुम्हार, सांनां – एक साथ मिलाकर।
सरलार्थ: कबीर कहते हैं कि हमने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। जो लोग उसे दो (अलग-अलग) मानते हैं, उनके लिए ही नरक की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को नहीं पहचाना है। वे तर्क देते हैं कि संपूर्ण संसार में एक ही हवा बहती है, एक ही जल है और एक ही प्रकाश (ईश्वरीय ज्योति) सब में समाया हुआ है। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार सभी प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व से सभी प्राणियों का निर्माण किया है।
पंक्तियाँ 5-8: “जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै… काहे रे नर गरबांनां॥”
शब्दार्थ: बाढ़ी – बढ़ई, काष्ट – लकड़ी, अगिनि – अग्नि, घटि – हृदय, अंतरि – अंदर, सरूपै – स्वरूप, लुभांनां – मोहित होना, गरबांनां – गर्व करना।
सरलार्थ: कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार यह शरीर नश्वर है, किंतु इसके अंदर व्याप्त आत्मा (परमात्मा का अंश) अजर-अमर है। वह परमात्मा सभी के हृदयों में व्याप्त है, भले ही उसने अलग-अलग स्वरूप धारण कर रखे हों। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य! तू इस सांसारिक माया को देखकर क्यों मोहित हो रहा है और इस नश्वर शरीर पर क्यों गर्व करता है?
पंक्तियाँ 9-10: “निरभै भया कछू नहिं ब्यापै… कहै कबीर दिवांनां॥”
शब्दार्थ: निरभै – निर्भय, ब्यापै – सताता है, दिवांनां – दीवाना, प्रेमी।
सरलार्थ: कबीर कहते हैं कि जब व्यक्ति मोह-माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह निर्भय हो जाता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। ईश्वर का दीवाना (प्रेमी) कबीर यह सत्य कह रहा है।
3. सौंदर्य बोध (Elaborate – 10 मिनट)
भाव पक्ष: इस पद में कबीर का अद्वैतवादी दर्शन स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और एकता का समर्थन किया है तथा सांसारिक मोह-माया और अहंकार को व्यर्थ बताया है। यह पद एक गहरा दार्शनिक और सामाजिक संदेश देता है।
कला पक्ष:
- भाषा: सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द हैं।
- अलंकार: ‘एक एक’ में यमक अलंकार है (पहले ‘एक’ का अर्थ संख्या और दूसरे का ‘परमात्मा’)। ‘काष्ट ही काटै’ में अनुप्रास अलंकार है। बढ़ई और कुम्हार का उदाहरण देने के कारण दृष्टांत अलंकार है।
- शैली: उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है।
- छंद: पद (गेय) छंद है।
4. मूल्यांकन (Evaluate – 10 मिनट)
कक्षा-कार्य: छात्रों से पूछें: ‘कबीर ने ईश्वर की एकता को सिद्ध करने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए हैं?’ और ‘बढ़ई और अग्नि का उदाहरण क्यों दिया गया है?’
गृहकार्य: NCERT अभ्यास के प्रश्न संख्या 1 और 3 तथा RBSE परीक्षा केंद्रित अभ्यास से सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न हल करने के लिए दें।
NCERT अभ्यास-प्रश्नों के विस्तृत हल
प्रश्न 1: कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं?
उत्तर: कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
- समान तत्व: कबीर कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही ईश्वरीय ज्योति सबमें व्याप्त है।
- कुम्हार का उदाहरण: जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व (पंचतत्व) से सभी प्राणियों की रचना की है।
- बढ़ई का उदाहरण: जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, पर उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा अमर रहती है, जो परमात्मा का ही अंश है।
इन तर्कों से वे सिद्ध करते हैं कि ईश्वर एक है और सभी प्राणियों में उसी का वास है।
प्रश्न 2: मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है?
उत्तर: कबीर के दर्शन और भारतीय मान्यता के अनुसार, मानव शरीर का निर्माण पाँच मूल तत्वों से हुआ है। ये पंच तत्व हैं- अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। कबीर ने अपने पद में ‘एकै खाक’ कहकर पृथ्वी तत्व की ओर संकेत किया है।
प्रश्न 3: ‘जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै अगिनि न काटै कोई। सब घटि अंतरि तूँही व्यापक धरै सरूपै सोई॥’ इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है?
उत्तर: इन पंक्तियों के आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप निम्नलिखित है:
- अविनाशी और अजर-अमर: ईश्वर अग्नि के समान अविनाशी है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, पर अग्नि को नहीं, वैसे ही मानव शरीर नश्वर है, पर उसमें व्याप्त आत्मा (ईश्वर) अमर है।
- सर्वव्यापक: ईश्वर ‘सब घटि अंतरि’ अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय में व्याप्त है।
- एकरूप: भले ही संसार में प्राणियों के रूप अलग-अलग (‘धरै सरूपै सोई’) हों, किंतु उन सब में एक ही परमात्मा का वास है।
अतः, कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक, अविनाशी, निराकार और एक है।
प्रश्न 4: कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है?
उत्तर: कबीर ने स्वयं को ‘दीवाना’ इसलिए कहा है क्योंकि वे सांसारिक मोह-माया, आडंबरों और भेदभाव से परे होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। ‘दीवाना’ का अर्थ है- किसी के प्रेम में पागल। कबीर ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं। उन्होंने ईश्वर के वास्तविक, निर्गुण और निराकार स्वरूप को पहचान लिया है। इस सत्य को जानने के बाद वे निर्भय हो गए हैं और दुनिया की परवाह किए बिना अपनी बात कहते हैं। आम सांसारिक लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए वे स्वयं को ईश्वर का दीवाना कहते हैं।
RBSE परीक्षा-केंद्रित अभ्यास
कवि परिचय (उत्तर सीमा 80 शब्द)
प्रश्न: कवि कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए।
उत्तर: कबीर भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद, धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों पर गहरा प्रहार किया। वे प्रेम, सद्भाव और समानता के पक्षधर थे। उनकी भाषा जनसामान्य की ‘सधुक्कड़ी’ भाषा है, जिसमें सरलता और प्रभाव है। अपनी बात को सीधे और दो टूक ढंग से कहने के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें ‘वाणी का डिक्टेटर’ कहा है। उनकी वाणियों का संग्रह ‘बीजक’ नामक ग्रंथ में संकलित है।
सप्रसंग व्याख्या
पद: “जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटै… कहै कबीर दिवांनां॥”
संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग-1’ में संकलित भक्तिकाल के निर्गुण संत कवि कबीर द्वारा रचित ‘सबद’ से उद्धृत है।
प्रसंग: यहाँ कबीर ने आत्मा की अमरता और परमात्मा की सर्वव्यापकता को सिद्ध करते हुए मनुष्य को सांसारिक मोह-माया और अहंकार से दूर रहने का उपदेश दिया है।
व्याख्या: कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, पर उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार यह शरीर नश्वर है किंतु इसके भीतर की आत्मा अमर है। वह परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, भले ही उनके बाहरी स्वरूप भिन्न हों। हे मनुष्य! तू इस नश्वर संसार को देखकर क्यों मोहित होता है और क्यों व्यर्थ गर्व करता है? जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर निर्भय हो जाता है, उसे कोई भय नहीं सताता। कबीर जैसा ईश्वर का दीवाना यही सत्य कह रहा है।
विशेष: (1) आत्मा की अमरता का सुंदर प्रतिपादन। (2) दृष्टांत अलंकार का प्रयोग। (3) सधुक्कड़ी भाषा। (4) उपदेशात्मक शैली।
बहुचयनात्मक प्रश्न (MCQ)
1. कबीर के अनुसार, ईश्वर को दो मानने वालों को क्या प्राप्त होता है?
2. कबीर ने अविनाशी तत्व किसे माना है?
अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 20 शब्द)
प्रश्न 1: कबीर ने संसार को किसमें मोहित बताया है?
उत्तर: कबीर के अनुसार, संसार सांसारिक मोह-माया और झूठे आडंबरों को देखकर उसमें मोहित हो रहा है।
प्रश्न 2: ‘एकै कोहरा सांनां’ पंक्ति का क्या आशय है?
उत्तर: इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने सभी प्राणियों को एक ही तत्व से बनाया है।
लघूत्तरात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 40 शब्द)
प्रश्न 1: ‘हम तौ एक एक करि जांनां’ पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: इस पद का प्रतिपाद्य ईश्वर की एकता को सिद्ध करना है। कबीर ने विभिन्न तर्कों और उदाहरणों से यह स्थापित किया है कि परमात्मा एक है और वह सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का खंडन करते हुए मनुष्य को अहंकार और मोह-माया त्यागकर निर्भय होने का संदेश दिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
निर्गुण भक्ति क्या है?
निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार, अरूप, अजन्मा और सर्वव्यापक स्वरूप की उपासना है। इसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अवतारवाद का विरोध किया जाता है। कबीर इसी भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, जो मानते थे कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, उसे मंदिरों या मस्जिदों में खोजने की आवश्यकता नहीं है।
कबीर ने ‘दोजग’ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है?
कबीर ने ‘दोजग’ (नरक) शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो ईश्वर को एक न मानकर उसे अलग-अलग (जैसे- हिंदू का राम, मुसलमान का रहीम) रूपों में बाँटते हैं। कबीर के अनुसार, जो लोग इस सत्य को नहीं पहचानते कि ईश्वर एक है, वे अज्ञानता में जीते हैं और यही उनके लिए नरक की स्थिति है।
कबीर की भाषा को ‘सधुक्कड़ी’ क्यों कहा जाता है?
कबीर एक संत थे और वे जगह-जगह घूमकर ज्ञान प्राप्त करते और उपदेश देते थे। इस कारण उनकी भाषा पर विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों का प्रभाव पड़ा। उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इसी मिश्रित भाषा को ‘सधुक्कड़ी’ या ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा जाता है।
हम आशा करते हैं कि कबीर के पद पर आधारित यह विस्तृत पाठ योजना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस Kabir Path Yojana को शिक्षकों और विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि आपको एक ही स्थान पर संपूर्ण शिक्षण और परीक्षा सामग्री मिल सके। कबीर का दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।