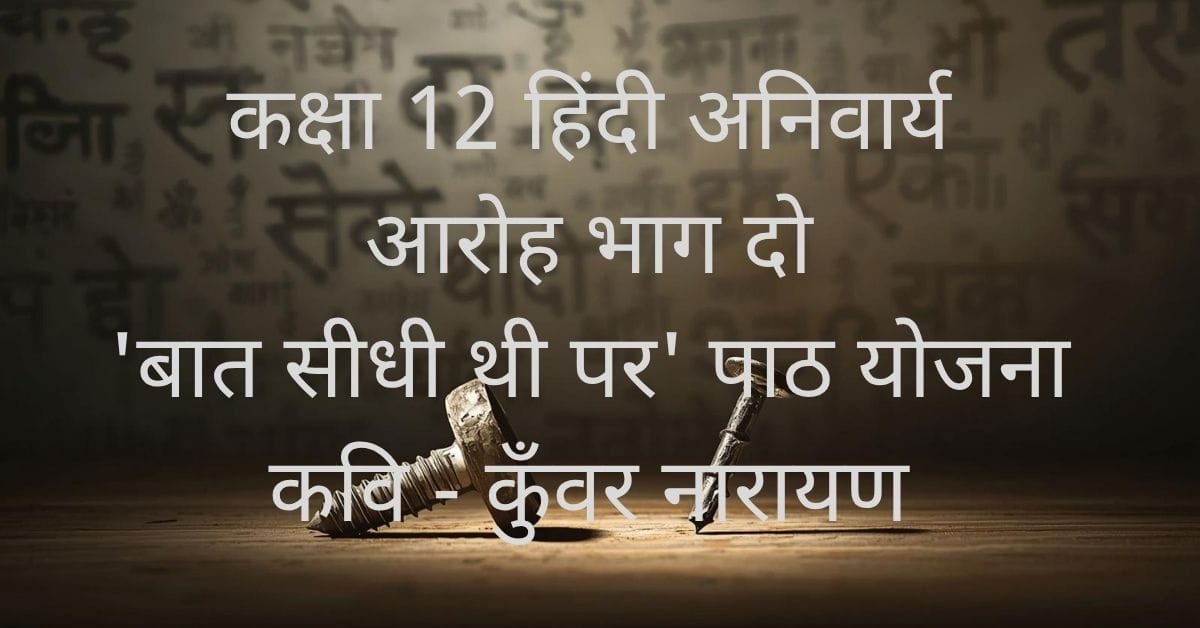बात सीधी थी पर पाठ योजना | Baat Sidhi Thi Par Path Yojana | आरोह भाग-2 | कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य
नमस्कार शिक्षक साथियों! ‘शिक्षक कॉर्नर’ में आपका स्वागत है। आज हम RBSE/CBSE कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक ‘आरोह भाग-2’ के पाठ 3 से कवि “कुँवर नारायण” की दूसरी प्रसिद्ध कविता ‘बात सीधी थी पर’ के लिए एक विस्तृत और गहन पाठ योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। यह Baat Sidhi Thi Par Path Yojana भाषा की सहजता और जटिलता के द्वंद्व को समझने में आपके कक्षा शिक्षण को आसान बनाएगी। इसमें आपको विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य, NCERT हल और परीक्षा-केंद्रित अभ्यास जैसी हर आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर मिलेगी।
इस लेख में आप क्या पढ़ेंगे
पाठ अवलोकन
| विवरण | जानकारी |
| कक्षा | 12 |
| विषय | हिंदी (अनिवार्य) |
| पुस्तक | आरोह भाग-2 (काव्य खंड) |
| पाठ | 3. बात सीधी थी पर |
| कवि | कुँवर नारायण |
| अनुमानित समय | 45 मिनट (1 कालांश) |
शैक्षणिक उद्देश्य एवं सामग्री
सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)
- विद्यार्थी कथ्य और माध्यम (भाषा) के संबंध को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी भाषा की सहजता और जटिलता के बीच के अंतर का विश्लेषण कर सकेंगे।
- विद्यार्थी यह समझ सकेंगे कि कैसे दिखावे और पांडित्य-प्रदर्शन के चक्कर में सीधी बात भी प्रभावहीन हो जाती है।
- विद्यार्थी कविता में प्रयुक्त ‘पेंच’, ‘कील’, ‘चूड़ी’ जैसे बिंबों की सार्थकता को समझ सकेंगे।
आवश्यक सामग्री (Required Materials)
- पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग-2’
- श्यामपट्ट/व्हाइटबोर्ड और मार्कर/चॉक
- पेंचकस, पेंच और कील जैसे वास्तविक उपकरण (वैकल्पिक, बिंब समझाने के लिए)
कवि परिचय: कुँवर नारायण
1. जीवन परिचय
कुँवर नारायण (जन्म: 19 सितंबर, 1927; निधन: 2017) नयी कविता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उत्तर प्रदेश में जन्मे कुँवर नारायण को नागर संवेदना का कवि माना जाता है। उन्होंने 1950 के आसपास काव्य-लेखन की शुरुआत की और अपनी एक अलग पहचान बनाई।
2. साहित्यिक परिचय
कुँवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ़-सुथरापन है। जीवन को समग्र रूप से समझने वाला एक खुलापन उनके कवि-स्वभाव की मूल विशेषता है। ‘आत्मजयी’ जैसे प्रबंध काव्य रचकर उन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की।
3. प्रमुख रचनाएँ
काव्य संग्रह: चक्रव्यूह (1956), परिवेश: हम-तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों।
प्रबंध काव्य: आत्मजयी।
कहानी संग्रह: आकारों के आस-पास।
4. प्रमुख सम्मान
उन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कबीर सम्मान और भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ (2005) से सम्मानित किया गया।
5. भाषा-शैली
कुँवर नारायण की भाषा और विषय में विविधता है। उनकी भाषा में संयम और साफ-सुथरापन है। वे सीधी घोषणाओं और फैसलों से बचते हैं। उनकी कविताओं के बीज शब्द हैं- संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता।
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (कक्षा के लिए विस्तृत गाइड)
1. पूर्व ज्ञान से जोड़ना (Engage – 5 मिनट)
कक्षा की शुरुआत इन प्रश्नों से करें ताकि विषय के प्रति छात्रों की रुचि जागृत हो सके:
- क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहना कुछ चाहते थे, पर गलत शब्दों के चुनाव से उसका अर्थ कुछ और ही निकल गया?
- सरल भाषा में अपनी बात कहना बेहतर है या कठिन शब्दों का प्रयोग करके? क्यों?
- ‘पेंच कसने’ और ‘कील ठोंकने’ में क्या अंतर होता है?
2. पाठ की प्रस्तुति (Explore & Explain – 20 मिनट)
सस्वर वाचन: उचित हाव-भाव, लय और आरोह-अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करें।
पद्यांश-वार विस्तृत व्याख्या:
पद्यांश 1: “बात सीधी थी पर… पेचीदा होती चली गई।”
सरलार्थ: कवि कहते हैं कि वे एक बहुत ही सीधी और सरल बात कहना चाहते थे, लेकिन उसे अधिक प्रभावी बनाने के चक्कर में वे भाषा की जटिलता में फँस गए। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शब्दों को बदला, वाक्यों को तोड़ा-मरोड़ा और घुमाया-फिराया। वे चाहते थे कि या तो उनकी बात का सही अर्थ निकल आए या फिर वह भाषा के इस जंजाल से मुक्त हो जाए। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ; भाषा के साथ-साथ उनकी सीधी-सी बात भी और अधिक उलझती चली गई।
पद्यांश 2: “सारी मुश्किल को… बेकार घूमने लगी!”
सरलार्थ: कवि कहते हैं कि वे समस्या को धैर्य से समझने के बजाय उसे और जटिल बनाते जा रहे थे। वे बात रूपी पेंच को खोलने के बजाय उसे जबरदस्ती कसते जा रहे थे। उनके इस भाषाई करतब पर दर्शक (तमाशबीन) उनकी प्रशंसा कर रहे थे और ‘वाह-वाह’ कर रहे थे, जिससे कवि को और बढ़ावा मिल रहा था। आखिरकार, वही हुआ जिसका डर था। अधिक ज़ोर-ज़बरदस्ती करने से बात का मूल प्रभाव (चूड़ी) नष्ट हो गया और वह भाषा में प्रभावहीन होकर बेकार घूमने लगी, अर्थात् कथ्य और भाषा का संबंध टूट गया।
पद्यांश 3: “हार कर मैंने उसे… कभी नहीं सीखा?”
सरलार्थ: जब कवि हर तरह से असफल हो गए, तो उन्होंने हारकर उस प्रभावहीन बात को कील की तरह उसी जगह पर जबरदस्ती ठोंक दिया। ऊपर से तो वह ठीक-ठाक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें न तो कोई कसावट थी और न ही कोई ताकत। अंत में, बात ने ही एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछा, जो अपनी इस असफलता पर पसीना पोंछ रहे थे – “क्या तुमने भाषा को सरलता और सहजता से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा?” यह प्रश्न कवि के लिए एक बड़ी सीख थी।
3. सौंदर्य बोध (Elaborate – 10 मिनट)
भाव पक्ष: यह कविता ‘कथ्य’ और ‘माध्यम’ के द्वंद्व को उजागर करती है। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कविता या किसी भी अभिव्यक्ति का सौंदर्य भाषा के आडंबर में नहीं, बल्कि भावों की सहज प्रस्तुति में है। जब भाषा को अनावश्यक रूप से जटिल बनाया जाता है, तो वह मूल बात के प्रभाव को ही नष्ट कर देती है।
कला पक्ष:
- भाषा: सरल, सहज खड़ी बोली, जिसमें उर्दू के शब्द (बेतरह, करतब, तमाशबीन) भी शामिल हैं।
- बिंब योजना: कवि ने ‘पेंच’, ‘चूड़ी’, ‘कील’ जैसे ठोस (मूर्त) बिंबों के माध्यम से ‘बात’ जैसे अमूर्त भाव को साकार कर दिया है।
- अलंकार: ‘बात की चूड़ी मर गई’ में रूपक अलंकार है। ‘बात’ का मानवीकरण एक शरारती बच्चे के रूप में किया गया है।
- शैली: मुक्त छंद में लिखी गई आत्मकथात्मक शैली है।
4. मूल्यांकन (Evaluate – 10 मिनट)
कक्षा-कार्य: छात्रों से पूछें: ‘बात की चूड़ी मर जाने’ का क्या परिणाम हुआ? कवि को तमाशबीनों की वाह-वाही क्यों मिल रही थी?
गृहकार्य: NCERT अभ्यास के प्रश्न संख्या 5, 6, और 7 तथा RBSE परीक्षा केंद्रित अभ्यास से सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न हल करने के लिए दें।
NCERT अभ्यास-प्रश्नों के विस्तृत हल
प्रश्न 5: ‘भाषा को सहूलियत से बरतने’ से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: ‘भाषा को सहूलियत से बरतने’ का अभिप्राय है भाषा का प्रयोग आडंबर या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भावों की सहज और सीधी अभिव्यक्ति के लिए करना। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बात कहने के लिए अनावश्यक रूप से कठिन, जटिल और बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शब्द और वाक्य-रचना भाव को सबसे सरलता और स्पष्टता से व्यक्त कर सके, उसी का प्रयोग करना चाहिए। भाषा को साधन बनाना चाहिए, साध्य नहीं।
प्रश्न 6: बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में ‘सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है’ कैसे?
उत्तर: बात (कथ्य) और भाषा (माध्यम) का गहरा संबंध है। भाषा के बिना बात को व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब लेखक या वक्ता अपनी विद्वता दिखाने या अपनी बात को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा को अनावश्यक रूप से अलंकृत और जटिल बना देता है, तो ‘सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है’। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाठक या श्रोता का ध्यान मूल बात से हटकर भाषा के बाहरी स्वरूप पर अटक जाता है। शब्दों के आडंबर में मूल अर्थ खो जाता है, जिससे बात स्पष्ट होने के बजाय और भी उलझ जाती है, जैसा कि कवि के साथ इस कविता में हुआ।
प्रश्न 7: बात (कथ्य) के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों/मुहावरों से मिलान करें।
उत्तर: उचित मिलान इस प्रकार है:
(क) बात की चूड़ी मर जाना → बात का प्रभावहीन हो जाना
(ख) बात की पेंच खोलना → बात को सहज और स्पष्ट करना
(ग) बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना → बात का पकड़ में न आना
(घ) पेंच को कील की तरह ठोंक देना → बात में कसावट का न होना
(ङ) बात का बन जाना → कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना
RBSE परीक्षा-केंद्रित अभ्यास
कवि परिचय (उत्तर सीमा 80 शब्द)
प्रश्न: कवि कुँवर नारायण का साहित्यिक परिचय दीजिए।
उत्तर: कुँवर नारायण (1927-2017) ‘नयी कविता’ दौर के प्रमुख नागर संवेदना के कवि हैं। उन्होंने ‘चक्रव्यूह’, ‘इन दिनों’ जैसे काव्य संग्रह और ‘आत्मजयी’ जैसा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचा। उनकी कविता में वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ़-सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी विशेषता है। जीवन को समग्रता में देखने की खुली दृष्टि के कारण उनकी कविताओं में संशय और प्रश्नाकुलता के भाव मिलते हैं। उन्हें साहित्य अकादेमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मानों से अलंकृत किया गया।
सप्रसंग व्याख्या
पद्यांश: “हार कर मैंने उसे कील की तरह… सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा?”
संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग-2’ में संकलित कवि कुँवर नारायण की कविता ‘बात सीधी थी पर’ से उद्धृत है।
प्रसंग: यहाँ कवि ने भाषा की जटिलता में उलझकर अपनी बात का प्रभाव खो देने के बाद की अपनी हताशा और आत्म-ग्लानि को व्यक्त किया है।
व्याख्या: कवि कहते हैं कि जब वे अपनी सीधी बात को भाषा के आडंबर से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने हार मानकर उस प्रभावहीन बात को जबरदस्ती कविता में ठोंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई पेंच के न कसने पर कील ठोंक देता है। वह रचना ऊपर से तो कविता जैसी लग रही थी, पर उसमें भावों की कोई गहराई या कसावट नहीं थी। तब कवि को ऐसा लगा मानो बात ने ही एक शरारती बच्चे के रूप में उनसे पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा का प्रयोग सरलता और सहजता से करना नहीं सीखा।
विशेष: (1) भाषा सरल और व्यंग्यात्मक है। (2) ‘कील की तरह ठोंक देना’ में सटीक बिंब का प्रयोग है। (3) ‘बात’ का मानवीकरण किया गया है। (4) मुक्त छंद का प्रयोग है।
बहुचयनात्मक प्रश्न (MCQ)
1. ‘बात सीधी थी पर’ कविता में कवि किस चक्कर में फँस गए?
2. ‘बात की चूड़ी मर गई’ का क्या अर्थ है?
अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 20 शब्द)
प्रश्न 1: कवि ने अपनी बात को उलटा-पलटा, तोड़ा-मरोड़ा क्यों?
उत्तर: कवि ने अपनी बात को उलटा-पलटा, तोड़ा-मरोड़ा ताकि या तो बात का सही अर्थ प्रकट हो जाए या फिर वह भाषा की जटिलता से बाहर आ जाए।
प्रश्न 2: कवि पर तमाशबीनों की ‘वाह-वाह’ का क्या असर हुआ?
उत्तर: तमाशबीनों की ‘वाह-वाह’ सुनकर कवि को और प्रोत्साहन मिला और वे बात रूपी पेंच को खोलने के बजाय और अधिक कसते चले गए।
लघूत्तरात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 40 शब्द)
प्रश्न 1: ‘बात सीधी थी पर’ कविता क्या संदेश देती है?
उत्तर: यह कविता संदेश देती है कि हमें अपनी बात को सहज और सरल भाषा में कहना चाहिए। भाषा का प्रयोग भावों को स्पष्ट करने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। बनावटी और जटिल भाषा मूल अर्थ को नष्ट कर देती है।
प्रश्न 2: ‘पेंच को खोलने के बजाए उसे बेतरह कसता चला जा रहा था’ – पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: इस पंक्ति का आशय है कि कवि भाषा की समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और अधिक उलझा रहे थे। वे सही शब्दों का चुनाव करके बात को सरल बनाने की जगह, और भी कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे जटिल बनाते जा रहे थे।
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न (उत्तर सीमा 60-80 शब्द)
प्रश्न 1: ‘बात सीधी थी पर’ कविता के आधार पर बताएँ कि एक अच्छी कविता या अच्छी बात कैसे बनती है?
उत्तर: इस कविता के अनुसार, एक अच्छी कविता या अच्छी बात का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ने पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त मेहनत या ज़ोर-ज़बरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती। जब कथ्य के अनुरूप सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बात अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। भाषा को साधन समझना चाहिए, साध्य नहीं। भाषा पर अनावश्यक दबाव डालने से उसका मूल प्रभाव नष्ट हो जाता है।
प्रश्न 2: कवि ने ‘बात’ के लिए ‘पेंच’, ‘चूड़ी’ और ‘कील’ जैसे उपमानों का प्रयोग क्यों किया है? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: कवि ने ‘बात’ जैसे अमूर्त विषय को समझाने के लिए इन मूर्त उपमानों का प्रयोग किया है ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सकें। जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खाँचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ज़ोर-ज़बरदस्ती से ‘पेंच की चूड़ी’ मर जाती है, वैसे ही गलत शब्दों से ‘बात का प्रभाव’ नष्ट हो जाता है। और अंत में, जब बात प्रभावहीन हो जाती है तो उसे ‘कील की तरह ठोंक’ देना पड़ता है, जो ऊपर से तो ठीक लगती है पर उसमें कोई कसाव नहीं होता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
इस कविता का मुख्य संदेश क्या है?
इस कविता का मुख्य संदेश है कि हमें अपनी बात को सहज, सरल और सीधी भाषा में कहना चाहिए। भाषा का आडंबर और दिखावा मूल भाव को नष्ट कर देता है।
कवि ने ‘बात’ को एक ‘शरारती बच्चे’ की तरह क्यों कहा है?
कवि ने ‘बात’ को ‘शरारती बच्चे’ की तरह इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा आसानी से पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कवि की मूल बात भी भाषा के जाल में उलझकर उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अंत में, उसी बात ने बच्चे की तरह सहजता से कवि को उनकी गलती का एहसास कराया।
हम आशा करते हैं कि कुँवर नारायण की कविता ‘बात सीधी थी पर’ पर आधारित यह विस्तृत पाठ योजना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस Baat Sidhi Thi Par Path Yojana को भाषा और अभिव्यक्ति के जटिल संबंधों को सरलता से समझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।